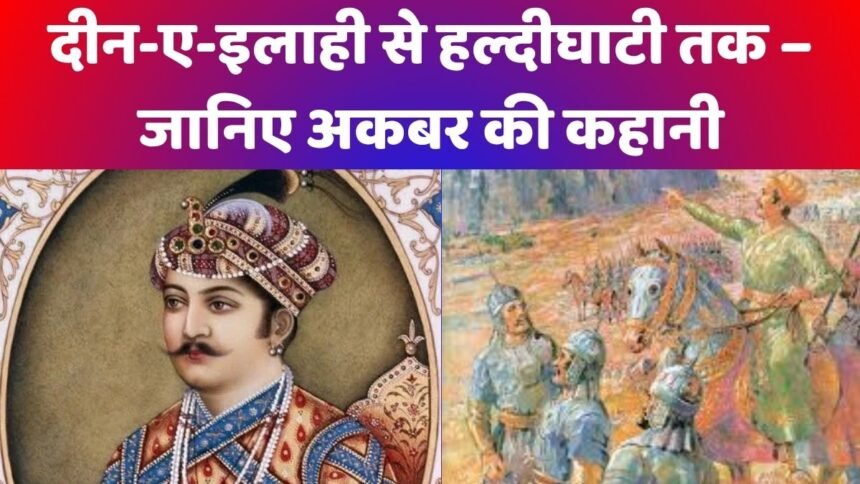अकबर का प्रारंभिक जीवन और उत्थान:-
अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट (अब पाकिस्तान में) हुआ था। उनके पिता सम्राट हुमायूं और माता हामिदा बानो बेगम थीं। जब अकबर का जन्म हुआ, तब हुमायूं अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष में थे। इसलिए अकबर का बाल्यकाल अस्थिरता और युद्धों के बीच बीता। हुमायूं की मृत्यु के बाद, 1556 में केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली। उस समय उसका संरक्षक बैरम खाँ था, जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई (1556) में हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराकर अकबर के शासन की नींव मजबूत की।
- अकबर का प्रारंभिक जीवन और उत्थान:-
- साम्राज्य विस्तार और विजय अभियान:-
- अकबर के प्रमुख युद्ध:-
- अकबर की धार्मिक नीति और ‘दीन-ए-इलाही’:-
- 4.दीन-ए-इलाही पर विवाद:-
- प्रशासनिक संरचना और नवरत्नों की भूमिका:-
- कला, संस्कृति और वास्तुकला में योगदान:-
- सामाजिक दृष्टिकोण और महिलाओं की स्थिति:-
- अकबर की मृत्यु और विरासत:-
- निष्कर्ष : एक युग पुरुष की प्रेरणादायक गाथा:-
बैरम खाँ की मृत्यु के बाद, अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और धीरे-धीरे एक महान प्रशासक और विजेता बनकर उभरा। उसने एक के बाद एक कई राज्यों को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया और अपने शासन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैलाया। प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों ने अकबर को राजनीतिक दूरदर्शिता, साहस और निर्णय क्षमता से परिपूर्ण शासक बनने में सहायता की।
-
साम्राज्य विस्तार और विजय अभियान:-
अकबर का शासनकाल भारत के भूगोलिक मानचित्र को बदलने वाला सिद्ध हुआ। उसने राजपूताने से लेकर गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन तक अपने विजय अभियानों से मुग़ल साम्राज्य को विशालतम स्वरूप दिया। राजपूतों के साथ अकबर की नीति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उसने बलपूर्वक नहीं, बल्कि सहमति और विवाह-संबंधों के माध्यम से कई राजपूत रियासतों को अपने अधीन किया।
अकबर ने चित्तौड़, रणथंभौर, कलिंजर, गुजरात और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीता। 1576 की हल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में महाराणा प्रताप से मुकाबला किया, हालाँकि यह युद्ध पूर्ण विजय नहीं थी, फिर भी मुग़ल प्रभुत्व राजस्थान में स्थापित हो गया। दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों पर भी उसकी निगाह रही, हालांकि इन क्षेत्रों में उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली।
इन युद्ध अभियानों की सफलता ने न केवल साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत कीं, बल्कि मुग़ल प्रशासन और संस्कृति को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया। इसके साथ ही, अकबर की सैन्य रणनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति ने उसे एक अत्यंत सफल सम्राट बना दिया।
अकबर के प्रमुख युद्ध:-
मुगल सम्राट अकबर (1556–1605) न केवल एक कुशल प्रशासक था, बल्कि एक महान सेनानायक भी था। उसने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और भारत के बड़े भूभाग को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। अकबर की युद्धनीति में कूटनीति और ताकत दोनों का संतुलन था।
- पानीपत का द्वितीय युद्ध (1556): अकबर का पहला बड़ा युद्ध था, जो हेमू (हेमचंद्र विक्रमादित्य) के विरुद्ध लड़ा गया। बैरम ख़ाँ के नेतृत्व में अकबर की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और दिल्ली की गद्दी को सुरक्षित किया।
- मालवा पर आक्रमण (1561): बाज बहादुर को हराकर अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद मालवा मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया।
- गुजरात अभियान (1572-1573): गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फर शाह को हराकर अकबर ने इस समृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। चम्पानेर और अहमदाबाद मुगलों के अधीन आ गए।
- रणथंभौर और चितौड़ का युद्ध (1567–1569): राणा उदय सिंह की अनुपस्थिति में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मावती की जौहर के ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़े इस किले को जीत लिया। रणथंभौर दुर्ग को भी जीतकर अकबर ने राजपूतों पर प्रभाव जमा लिया।
- बीजनौर और काबुल अभियान: अफगान विद्रोहियों को दबाने के लिए अकबर ने बीजनौर और पश्तून क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अभियान चलाए।
- बंगाल और उड़ीसा युद्ध (1574-1576): बंगाल के सुल्तान दाउद खान को हराकर अकबर ने पूर्वी भारत को अपने अधीन किया।
- राणा प्रताप से हल्दीघाटी का युद्ध (1576): यह युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। हालांकि अकबर ने विजय प्राप्त की, परंतु राणा प्रताप की वीरता आज भी याद की जाती है।
अकबर के इन युद्धों ने मुगल साम्राज्य को अखिल भारतीय रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
-
अकबर की धार्मिक नीति और ‘दीन-ए-इलाही’:-
अकबर की धार्मिक नीति उसे अन्य सम्राटों से अलग बनाती है। उसने अपनी धार्मिक सोच को सीमित नहीं रखा, बल्कि विविध धर्मों के तत्वों को आत्मसात करने की कोशिश की। प्रारंभ में एक कट्टर मुस्लिम के रूप में शुरुआत करने वाले अकबर ने धीरे-धीरे हिंदू, जैन, बौद्ध और ईसाई विचारधाराओं को भी समझने का प्रयास किया।
1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ‘इबादतखाना’ की स्थापना की, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। इन चर्चाओं से प्रभावित होकर 1582 में अकबर ने ‘दीन-ए-इलाही’ नामक एक नई धार्मिक विचारधारा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के श्रेष्ठ गुणों को मिलाकर एक वैश्विक नैतिक व्यवस्था स्थापित करना था। हालांकि यह पंथ बहुत कम लोगों द्वारा अपनाया गया और मुस्लिम उलेमाओं ने इसका विरोध भी किया।
अकबर ने जज़िया कर (गैर-मुस्लिमों पर लगने वाला कर) समाप्त किया, मंदिरों को संरक्षण दिया और विभिन्न जातियों व धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया। इससे उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु शासक के रूप में उभरी, जो भारतीय इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है।
4.दीन-ए-इलाही पर विवाद:-
अकबर द्वारा 1582 ई. में स्थापित किया गया दीन-ए-इलाही एक नया धार्मिक मत था, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धांतों का समन्वय करके एक साझा आस्थावादी प्रणाली विकसित करना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्मों के नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों को सम्मिलित किया गया था। यद्यपि इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था, फिर भी इसे लेकर उस समय कई विवाद उत्पन्न हुए। इस धर्म की सबसे बड़ी आलोचना इस्लामी उलेमाओं और मौलवियों ने की, जिन्होंने इसे इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। उन्होंने अकबर पर “पैगंबर बनने की आकांक्षा” और शरिया से विचलन का आरोप लगाया। दूसरी ओर हिंदू पुरोहितों और पारंपरिक समाजों ने भी इसे संशय की दृष्टि से देखा। इसके अनुयायी बहुत कम थे, जिनमें अबुल फज़ल प्रमुख थे, और यह अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। आलोचकों का कहना था कि यह धार्मिक सुधार कम और राजनीतिक साधन अधिक था, जिससे अकबर अपनी सर्वोच्चता को धार्मिक स्तर पर भी स्थापित करना चाहता था। यद्यपि यह विचार सीमित रहा, लेकिन यह उस युग की धार्मिक उदारता और प्रयोगशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
प्रशासनिक संरचना और नवरत्नों की भूमिका:-
मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक स्वर्णिम युग माना जाता है। अकबर न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का संरक्षक भी था। उसकी राजसभा में नौ प्रमुख विद्वान और गुणी व्यक्ति थे, जिन्हें “नवरत्न” कहा जाता है। इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और हास्यबुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। तानसेन, जिन्हें संगीत का देवता कहा जाता है, अकबर के दरबार में संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे। अबुल फज़ल और फैजी दो भाई थे—अबुल फज़ल अकबरनामा और आइने अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखक थे, जबकि फैजी एक महान कवि थे। राजा टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था को संगठित कर एक प्रभावी कर प्रणाली स्थापित की। राजा मानसिंह एक वीर सेनापति थे और कई युद्धों में अकबर के भरोसेमंद सहयोगी रहे। मुल्ला दो प्याज़ा को अकबर के सलाहकारों में हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। फकीर अज़ियाउद्दीन एक आध्यात्मिक और धार्मिक सलाहकार थे। रहीम (अब्दुर रहीम ख़ान-ए-ख़ाना) एक महान कवि और साहित्यकार थे, जिनकी दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। ये नवरत्न अकबर के शासन को सशक्त और बहुआयामी बनाने में सहायक सिद्ध हुए, और उनके योगदान से अकबर का दरबार ज्ञान, कला और प्रशासन का केंद्र बन गया।
कला, संस्कृति और वास्तुकला में योगदान:-
अकबर का शासनकाल भारतीय कला और संस्कृति के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। उसने भारतीय, फारसी और इस्लामी तत्वों का समावेश करते हुए एक नई मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। अकबर स्वयं निरक्षर था, परंतु उसे विद्वानों और साहित्य से अत्यंत प्रेम था।
उसने फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और लाहौर किला जैसी स्थापत्य कृतियाँ बनवायीं, जो आज भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण मानी जाती हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, पंच महल और दीवान-ए-खास मुग़ल वास्तुकला की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।
संगीत के क्षेत्र में अकबर ने तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ को संरक्षण दिया, जिनकी रचनाएँ आज भी भारतीय संगीत में आदर्श मानी जाती हैं। इसके अलावा फारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाया गया और ‘अकबरनामा’ तथा ‘आईन-ए-अकबरी’ जैसे ग्रंथों की रचना करवाई गई, जो इतिहास के अमूल्य दस्तावेज हैं।
सामाजिक दृष्टिकोण और महिलाओं की स्थिति:-
अकबर ने समाज सुधार की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया, बाल विवाह पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और पर्दा प्रथा पर नियंत्रण करने जैसे निर्णयों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए।
अकबर ने हर धर्म और जाति की महिलाओं को न्याय देने की नीति अपनाई। दरबार में रानियों को भी कुछ मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। वह रानियों की शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने शाही हरम में शिक्षिका नियुक्त की थी।
अकबर की हरम नीति भी अन्य सम्राटों से भिन्न थी। उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर उन्हें केवल प्रतीक नहीं, बल्कि सम्मानजनक दर्जा भी प्रदान किया। यह नीति उसकी सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती है।
अकबर की मृत्यु और विरासत:-
अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी, जो उनके पोते शाहजहाँ के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। अकबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहाँगीर ने गद्दी संभाली।
अकबर की सबसे बड़ी विरासत उसका प्रशासनिक कौशल, धर्मनिरपेक्ष सोच, कलात्मक रुचि और लोगों को साथ लेकर चलने की नीति है। उसने भारत में एक साझा सांस्कृतिक चेतना की नींव रखी, जो आज भी भारतीय समाज की विविधता में एकता को दर्शाती है।
उसे ‘अकबर द ग्रेट’ कहा जाता है — यह उपाधि केवल उसकी सैन्य विजय के कारण नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों, धर्म-सहिष्णुता और जनकल्याणकारी कार्यों के कारण है।
निष्कर्ष : एक युग पुरुष की प्रेरणादायक गाथा:-
अकबर केवल एक विजेता नहीं था, वह एक दूरदर्शी, नीतिज्ञ, समाज-सुधारक और महान शासक था। उसने भारतीय इतिहास को न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी नई दिशा दी। उसका शासनकाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुजातीय भारत के लिए एक मिसाल बना।
आज जब हम विविधता और सह-अस्तित्व की बात करते हैं, तब अकबर का नाम एक प्रेरणा स्वरूप सामने आता है। उसकी नीतियाँ आज भी शांति, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की मिसाल हैं। वास्तव में, अकबर भारतीय इतिहास का वह सूर्य है, जिसकी रोशनी आज भी हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रकाशित करती है।
Also Read This – अमरोहा तेंदुआ: बांसखेड़ी गांव में दहशत, सीसीटीवी में कैद हुआ जंगली मेहमान