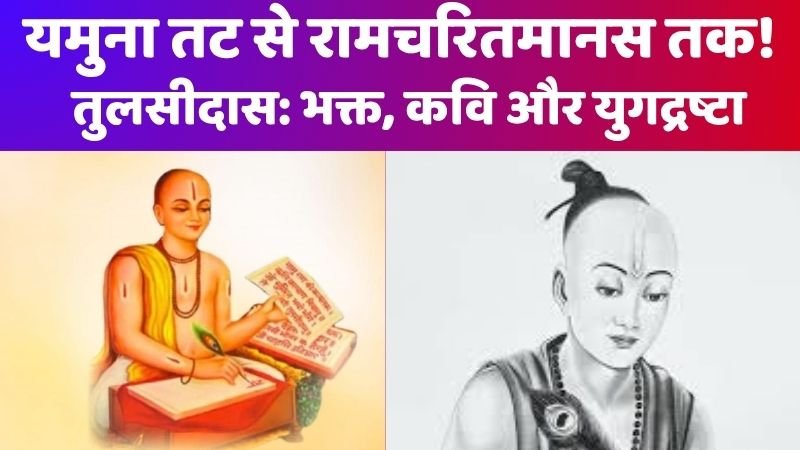यमुना तट जन्म: बालक रामबोला का आगमन
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म भारत के भक्ति युग का एक अविस्मरणीय अध्याय है। उन्होंने जन्म लिया श्रावण शुक्ल सप्तमी के पावन दिन, जो कि हिन्दू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। जन्म तिथि थी विक्रम संवत 1554, और स्थान था राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उनका जन्म यमुना तट के पास हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जब वह जन्मे, तो बालक के मुख से पहला शब्द निकला – “राम”, जिसे देखकर लोग चकित रह गए। इस कारण उन्हें रामबोला नाम दिया गया।
- यमुना तट जन्म: बालक रामबोला का आगमन
- गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण एवं प्रयाण दिवस
- बाल्यकाल से तपस्विता तक – रामबोला से गोस्वामी तुलसीदास:-
- विवाह, वैराग्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति:-
- रामचरितमानस की रचना – एक कालजयी महाकाव्य:-
- अन्य रचनाएँ और सामाजिक प्रभाव:-
- विक्रम संवत 1680 – देहावसान और अमरत्व:-
- निष्कर्ष: गोस्वामी तुलसीदास – युगों तक अमर:-
रामबोला एक साधारण बालक नहीं थे। वे बचपन से ही ईश्वरीय चेतना से परिपूर्ण थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म केवल भगवान राम के कार्यों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ ही समय बाद उनके माता-पिता का देहांत हो गया। उन्हें एक साधु नरहरिदास ने पालन-पोषण किया और उन्हें राम भक्ति की ओर प्रेरित किया।
गोस्वामी तुलसीदास के जन्म की कथा को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। उनका जन्म यमुना तट पर होना, उनका नाम रामबोला पड़ना, और उनका जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित होना – ये सभी बातें इस बात का संकेत हैं कि वे भगवान राम के कार्य हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण एवं प्रयाण दिवस
(स्वामी गोपाल आनंद बाबा)
श्री राम चरित मानस (तुलसीकृत रामायण) सहित अनेक ग्रंथों के रचियता गोस्वामी तुलसीदास का इस धरती पर अवतरण (जन्म) एवं महाप्रयाण (मृत्यु) दिवसों के बारे में निम्न दोहे उपलब्ध होते हैं।
पंदरह सौ चउवन बिषै, कालिन्दी के तीर।
सावन सुकला तीज शनि, तुलसी धरेऊसरीर।।
दूसरा- पंदरह सौ चउवन बिषै कालिन्दी के तीर। सावन सुकला, सप्तमी, तुलसी धरेउ सरीर।।
तथा संबत सोरह सौ असी, असी गंग के तीर।
सावन सुकल सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर।।
पहले दोहे में बताया गया है कि विक्रम संवत 1554 में श्रावण शुक्ल तृतीया दिन शनिवार को तुलसीदास (रामबोला) का जन्म हुआ। दूसरे में कहा गया है कि विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को कालिन्दी (श्रीयुमनानदी) के तट पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ।
तीसरे दोहे में ज्ञात कराया जा रहा है कि विक्रम संवत 1680 में काशी में गंगा जी के अस्सी घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने महाप्रयाण किया। अर्थात वे 1554 से 1680 तक कुल 126 वर्ष साक्षात सशरीर इस भूतल पर विद्यमान रहे।
तुलसीदास जी के समकालीन रहे बाबा बेनी माधव दास जी कृत एक मान्यता प्राप्त ग्रंथ ‘मूल गोसाई चरित’ में उन्होंने उनका अवतरण दिवस व वर्ष तथा स्थान संवत 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी यमुना तट माना है। वहीं इन्होंने ही श्री तुलसी चरित में कहा है कि उनकी परमधाम जाने की तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया दिन शनिवार संवत 1680, अस्सी गंग के तीर है। लेकिन ऊपर दिया गया दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, कि श्रावण शुक्ल सप्तमी वि.सं. 1680 में तुलसीदास जी ने शरीर त्यागा अर्थात सं. 1554 सावन सुदि सप्तमी एवं सं.1680 सावन सुदि सप्तमी जन्म एवं मृत्यु तिथि है। दोनों में जयन्ती व प्रयाण का दिवस एक ही तिथि में है। जैसा कि स्वामी रामतीर्थ के जन्म व निधन दिवस दीपावली (दिवाली) कार्तिक अमावस्या है। भगवान बुद्ध का जन्म व निधन दिन भी एक ही तिथि को माना जाता है। श्री गोस्वामी के शिष्य-परम्परागत पं. शिवलाल पाठक (काशी निवासी) जिन्होंने बाल्मीकि रामायण का संस्कृत भाष्य लिखा है, कृत श्री रामचरित मानस की ‘मानस मयंक’ नाम की टीका में भी बताया गया है कि श्रीगोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 (वि.) ही है। वे लिखते हैं – संवत 1554 में तुलसीदास जी का प्रगटीकरण हुआ और 5 वर्ष की आयु में अपने गुरु से उन्होंने राम कथा सुनी। पुन: दुबारा 40 वर्ष की आयु में वही कथा संतों से सुनी। पुन: उसको 77 वर्ष की आयु में संवत 1631 में प्रगट कर श्रीराम चरित मानस की रचना प्रारंभ की। इससे उसे भगवत-यश-रूप जल का चिराना कहा है। इस प्रकार 1554 में 77 वर्ष जोडऩे से संवत: 1631 हुआ। ‘संबत सोरह का एक तीसा। कर ऊ कथा हरि पद धरि सीसा’
पश्चात संवत 1680 में आप परमधाम सिधारे। इस प्रकार उन्होंने 126 वर्ष का दीर्घ जीवन व्यतीत किया। यहां एक और बात बताना आवश्यक है। ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ द्वारा प्रकाशित ‘श्री तुलसीदास ग्रन्थावली खण्ड 3’ के पृष्ठ 98 में जो बताया गया है वह भी श्रावण शुक्ल सप्तमी को जन्म बताता है।
बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित प्राचीन संशोधित ‘विनय पत्रिका’ में भी यही प्रमाण दिया गया है। इसमें पूज्य गोस्वामी जी के 36 वर्ष, 77 वर्ष और 98 वर्ष आयु के तीनों चित्र मुगल बादशाह अकबर के पुस्तकालय वाला, डाक्टर ग्रियर्सन की खोज में प्राप्त और काशी के अस्सी गंगा संगम के दिए गए हैं। उसमें भी यह दोहा अंकित है- ‘पंदरह सौ चउवन विषै, कालिन्दी के तीर। सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे सरीर’ अत: श्रावण शुक्ल सप्तमी ही गोस्वामी जी की जयन्ती है और पुण्यतिथि भी।
बाल्यकाल से तपस्विता तक – रामबोला से गोस्वामी तुलसीदास:-
बालक रामबोला का जीवन संघर्षों से भरा रहा। माता-पिता की मृत्यु के बाद उन्हें नरहरिदास ने आश्रय दिया और जीवन का उद्देश्य समझाया। नरहरिदास ने उन्हें काशी ले जाकर शिक्षा दी। वहां उन्होंने वेद, पुराण, व्याकरण, न्याय और दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इस काल में गोस्वामी तुलसीदास का वैराग्य और भक्ति और भी गहराती गई।
बाल्यकाल में ही वे साधु-संतों की संगति में रहने लगे और धर्म, कर्म और ज्ञान की बातें आत्मसात करने लगे। उनका व्यक्तित्व संयमित, सौम्य और तपस्वी था। वे समय-समय पर गांव-गांव जाकर रामकथा सुनाते, जिससे लोगों में धार्मिक जागृति फैलती। उनका जीवन बहुत ही अनुशासित और ब्रह्मचर्यपूर्ण था।
इस अवधि में उन्हें यह अनुभव हुआ कि संस्कृत में लिखे धार्मिक ग्रंथ आम जनता की पहुँच से दूर हैं। यह भावना उन्हें इस दिशा में सोचने को प्रेरित करती रही कि कैसे भगवान राम की महानता को जन-जन तक पहुँचाया जाए। यही विचार आगे चलकर उन्हें रामचरितमानस की रचना की ओर ले गया।
इस प्रकार बाल्यकाल में ही गोस्वामी तुलसीदास के भीतर वह चेतना विकसित हो चुकी थी, जिसने आगे चलकर उन्हें रामभक्ति आंदोलन का प्रमुख स्तंभ बना दिया। वे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक युगद्रष्टा, समाज सुधारक और संत थे।
विवाह, वैराग्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति:-
युवावस्था में गोस्वामी तुलसीदास ने एक सुशिक्षित और धार्मिक विचारों वाली स्त्री रत्नावली से विवाह किया। वे रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके साथ सुखमय जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ घटा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
एक बार रत्नावली अपने मायके गई हुई थीं। तुलसीदास उनसे मिलने के लिए रात में ही निकल पड़े, वर्षा और अंधकार से भयभीत न होकर नदी पार करके पहुँच गए। जब रत्नावली ने उन्हें अचानक अपने कक्ष में देखा तो आश्चर्यचकित होकर एक तीखा वाक्य कहा –
“लाज न आवत आपको, आए हौं राति अंधियारि।
अस्थि चर्ममय देह यह, ता सौं ऐसी प्रीति॥”
और फिर आगे जो कहा वह उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन गया –
“यदि तुम्हें इतनी ही प्रीति श्रीराम से होती, तो जीवन सफल हो जाता।”
इस वाक्य ने गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा को झकझोर दिया। वे उसी क्षण संसार को त्याग कर संन्यासी बन गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन, मोह, प्रेम और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त की और श्रीराम की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए।
अब वे रामबोला से पूर्ण रूप से गोस्वामी तुलसीदास बन चुके थे। काशी लौटकर उन्होंने राम नाम का प्रचार-प्रसार प्रारंभ किया, वन-वन जाकर कथा कीर्तन करने लगे और तपस्या में लीन हो गए। उनका जीवन अब भक्ति, ज्ञान और तप का पर्याय बन चुका था।
यह वह दौर था जब उन्होंने निश्चय किया कि भगवान श्रीराम के जीवन का संदेश केवल विद्वानों तक नहीं, बल्कि जन-जन तक पहुँचना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें भारत के सबसे महान ग्रंथों में से एक – रामचरितमानस – की रचना के लिए प्रेरित किया।
रामचरितमानस की रचना – एक कालजयी महाकाव्य:-
गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध और कालजयी कृति है – रामचरितमानस। यह ग्रंथ न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महान उपलब्धि है। इसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा ताकि आम जन इसे पढ़ और समझ सकें।
रामचरितमानस की रचना उन्होंने काशी में विक्रम संवत 1631 में आरंभ की और इसे सात वर्षों में पूर्ण किया। ग्रंथ के सात कांड हैं – बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इन कांडों के माध्यम से उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों, चरित्र, मर्यादा और नीति को जन-जन तक पहुँचाया।
गोस्वामी तुलसीदास का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने राम के जीवन को भारतीय जीवन मूल्यों का आधार बनाया। रामचरितमानस में उन्होंने राम को “मर्यादा पुरुषोत्तम” के रूप में प्रस्तुत किया। राम न केवल एक राजा थे, बल्कि वे नीति, धर्म और आदर्शों के प्रतीक थे।
उनकी यह रचना उस समय के समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों और आडंबरों को तोड़ती है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर केवल ब्राह्मणों या पंडितों के लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए हैं। रामचरितमानस ने समाज को एकजुट किया, भाषाई दीवारें गिराईं, और भक्ति को जन-जन तक पहुँचाया।
गोस्वामी तुलसीदास ने इस रचना के माध्यम से रामभक्ति आंदोलन को मजबूत किया। यह ग्रंथ आज भी घर-घर में पूजा जाता है, और इसकी चौपाइयाँ, दोहे और श्लोक आम जनमानस की जुबान पर हैं।
अन्य रचनाएँ और सामाजिक प्रभाव:-
गोस्वामी तुलसीदास ने केवल रामचरितमानस ही नहीं, बल्कि अनेक महान ग्रंथों की रचना की, जो भक्तिभाव, नीति, ज्ञान और साहित्यिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- हनुमान चालीसा:
यह ग्रंथ भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया है। इसकी 40 चौपाइयाँ आज भी भक्तों द्वारा नित्य पाठ के रूप में की जाती हैं। इसमें बल, बुद्धि, भक्ति और साहस की महिमा वर्णित है।
- विनय पत्रिका:
यह एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति आत्म समर्पण है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने विनय, दीनता और भगवान के प्रति अगाध प्रेम का अद्भुत चित्रण किया है।
- दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नहछू, जानकीमंगल, बारवै रामायण – ये सभी रचनाएँ उनके साहित्यिक कौशल और भक्ति के गहरे भाव को दर्शाती हैं।
इन रचनाओं के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह बताया कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और भक्ति है। उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों, वंचितों और अछूतों को भी भक्ति के समान अधिकार दिए।
वे समाज सुधारक भी थे, जो जात-पात और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध थे। उन्होंने राम नाम को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। उनके अनुसार –
“भजहु राम बिनु भावन संका। संतन कर यह लच्छन संका॥”
– जो राम का भजन करता है, वही सच्चा साधक है।
गोस्वामी तुलसीदास की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके काल में थी। उनका साहित्य, भक्ति और विचारधारा भारतीय समाज की रीढ़ बन चुका है।
विक्रम संवत 1680 – देहावसान और अमरत्व:-
गोस्वामी तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति, सेवा और प्रचार में लगा दिया। वे अंतिम वर्षों में काशी के अस्सीघाट पर निवास करते थे। वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय राम नाम के जाप में व्यतीत किया।
उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1680 में हुई। किंवदंती है कि जब वे मृत्यु के समीप थे, तो उन्होंने राम का नाम लेते हुए शांत भाव से अपने शरीर को त्याग दिया। उनके प्राण अंत में भगवान राम में लीन हो गए। उनकी समाधि आज भी काशी में तुलसीघाट पर स्थित है, जहाँ देशभर से श्रद्धालु पहुँचते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु मात्र एक संत का देह त्याग नहीं थी, बल्कि यह भारतीय भक्ति आंदोलन के एक युग का समापन था। वे अमर हो गए – अपनी रचनाओं, शिक्षाओं और आदर्शों के माध्यम से। आज भी जब कोई भक्त रामचरितमानस का पाठ करता है, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा बसती है।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में ही शक्ति है, त्याग में ही विजय है और साहित्य में ही समाज की आत्मा होती है। वे केवल एक कवि नहीं थे, वे एक जीवन-दर्शन थे।
निष्कर्ष: गोस्वामी तुलसीदास – युगों तक अमर:-
गोस्वामी तुलसीदास का जीवन एक प्रकाशपुंज था, जिसने अंधकार से भरे युग को धर्म, नीति और भक्ति की रोशनी से आलोकित कर दिया। उनका जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी, उनका जीवनकाल विक्रम संवत 1554 से 1680, उनका बाल्य नाम रामबोला, और उनका जन्मस्थान यमुना तट — ये सब कुछ एक दिव्य यात्रा के प्रतीक हैं।
उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर की आराधना है। उनकी रचनाएँ कालजयी हैं, और उनका प्रभाव सदियों तक जीवित रहेगा।
गोस्वामी तुलसीदास का नाम जब भी लिया जाएगा, वह हमें भक्ति, नीति और साहित्य की पराकाष्ठा की याद दिलाएगा। वे सच्चे अर्थों में भारत माता के पूज्य पुत्र हैं – संतों के शिरोमणि, भक्तों के मार्गदर्शक और साहित्य के महर्षि।
Also Read This – मध्यप्रदेश में कागजी सड़कें: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते विकास कार्य